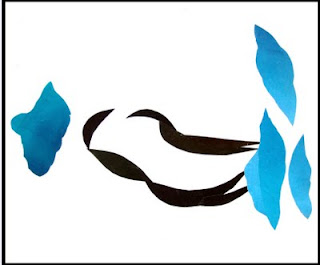पूर्वी कुमांऊ तथा पश्चिमी नेपाल की राजी जनजाति (वनरावतों) की बोली का अनुशीलन (अप्रकाशित शोध् प्रबंध) डॉ. शोभाराम शर्मा का एक महत्वपूर्ण काम है। उत्तराखंड के पौड़ी-गढ़वाल के पतगांव में 6 जुलाई 1933 को जन्मे डॉ। शोभाराम शर्मा 1992 में राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर से हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। 50 के दशक में डा। शोभाराम शर्मा ने अपना पहला लघु उपन्यास "धूमकेतु" लिखा था। पेशे से अध्यापक रहे डा.शर्मा ने अपनी रचनात्मकता का ज्यादातर समय भाषाओं के अध्ययन में लगाया है। सामान्य हिंदी, मानक हिंदी मुहावरा कोश (दो भाग), वर्गीकृत हिंदी मुहावरा कोश (दो भाग), वर्गीकृत हिंदी लोकोक्ति कोश (दो भाग) उनके इस काम के रूप में समय-समय पर प्रकाशित हुए हैं।
पिछलों दिनों उन्होंने संघर्ष की ऊर्जा से अनुप्राणित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के अनुवाद भी किए जो जल्द ही प्रकाशन की प्रक्रिया से गुजरकर पुस्तकाकार रूप में देखे जा सकेंगे। इसी कड़ी में "जब व्हेल पलायन करते हैं" एक महत्वपूर्ण कृति है। इससे पूर्व 'क्रांतिदूत चे ग्वेरा" (चे ग्वेरा की डायरी पर आधरित जीवनी) का हिन्दी अनुवाद, लेखन के प्रति डा.शोभाराम शर्मा की प्रतिबद्धता को व्यापक हिन्दी समाज के बीच रखने में उल्लेखनीय रहा है। इसके साथ-साथ डॉ. शोभाराम शर्मा ने ऐसी कहानियां लिखी हैं जिनमें उत्तराखंड का जनजीवन और इस समाज के अंतर्विरोध् बहुत सहजता के साथ अपने ऐतिहासिक संदर्भों में प्रस्तुत हुए हैं। उत्तराखंड की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामंतवाद के विरोध् की परंपरा पर लिखी उनकी कहानियां पाठकों में लोकप्रिय हैं।
वनरावतों पर लिखा उनका उपन्यास "काली वार-काली पार" जो प्रकाशनाधीन है, नेपाल के बदले हुए हालात और सामंतवाद के विरूद्ध संघर्ष की अवश्यमभाविता को समझने में मददगार है। प्रस्तुत है नेपाल के सीमांत में रहने वाली राजी जन जाति पर लिखे गए उनके इसी उपन्यास 'काली वार-काली पार" का एक छोटा सा अंश :
उपन्यास अंश
काली वार-काली पार
डॉ.शोभाराम शर्मा
उस साल चौमास (चातुर्मास) कुछ पहले ही बीत गया। आषाढ़-सावन में तो बारिश कुछ ठीक हुई, लेकिन भादो लगते ही न जाने क्यों रूठ गई। बादल आते, कुछ देर आंख-मिचौली खेलते और पिफर अंगूठा दिखाकर न जाने कहां गायब हो जाते। परिणाम यह हुआ कि हरी-भरी पफसल मुरझाने लगी। लगता था कि जैसे पफसल को पीलिया हो गया हो, धान, झंगोरा (सवां), मंडुवा में बालियां तो आ गई थीं, लेकिन ऐन मौके पर वर्षा बन्द हो गई। पुष्ट दानों का तो अब सवाल ही नहीं रहा। अदसार (अर्द्धसार) फसल हाथ लग जाए, बस वही बहुत था। नदी-घाटियों में जहां सिंचाई सुलभ थी, वहां तो अधिक नुकसान की सम्भावना कम ही थी। फ़िर भी आसमानी वर्षा की तो बात ही कुछ और है। उसके अभाव में वहां भी भरपूर फसल की आशा नहीं रही। ऊपर बसे गांवों का तो बहुत बुरा हाल था। मक्के में ठीक से दाने कहां से पड़ते जबकि पानी के अभाव में पौधे ही पीले पड़ने लगे थे। हर नई फसल के हाथ आने से पहले वैसे भी प्राय: हाथ तंग होता ही है। लेकिन जब अगली फसल के मारे जाने का दृश्य आंखों के सामने हो तो लोग कहां और किस ओर देखें। वनवासी राजियों की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। रोपाई, गुड़ाई और निराई के काम से जो थोड़ा बहुत अनाज मिला था वह भी समाप्ति पर था। जंगलों के बीच खील काटकर फसल बोई तो थी, लेकिन बालियां आने से पहले ही सूखने लगी थीं। गींठी (बाराही कन्द), तरुड़ आदि के कन्द अभी तैयार नहीं हुए थे। लाचारी में खोदकर लाते भी तो बेस्वाद खाए नहीं जाते थे।
चिफलतरा के गमेर को अपनी और अपने लोगों की चिन्ता खाए जा रही थी। मुखिया था लेकिन कोई राह नहीं सूझ पा रही थी। अपनी छानी के आगे सांदण के एक कुन्दे को बसूले से छील रहा था कि सामने फत्ते के खेत पर नजर पड़ी। फत्ते के गाय-बछड़े अनाज के पौधों को चट करने में लगे थे। गमेर ने फत्ते को आवाज दी -
फत्ते! अरे वा फत्ते!! गाय खुल गई है रे! बाहर तो आ।
फत्ते छानी से बाहर निकला और गाय-बछड़े हांकने के बजाय झंगोरे के दो-तीन अधमरे पौधे उखाड़कर गमेर के पास आकर बोला-
दाज्यू, गाय खुली नहीं, मैंने ही चरने छोड़ दी है। देखो, फसल तो पूरी चौपट हो चुकी है। सोचा, गाय-बछड़े ही अपना पेट भर लें
गमेर ने पौधे छूकर कहा-
ठीक कहते हो भाऊ, फसल तो सचमुच बर्बाद है, डंगरों के मतलब की ही रह गई है। सोचता हूं यहां से बाहर निकल जाते, लेकिन अभी तो कम-से-कम एक महीना बाकी है।
लेकिन तब तक जिन्दा भी रह पाएंगे दाज्यू? घास-पात खाकर कब तक निभेगी। शिकार-मछली का जुगाड़ भी ठीक से नहीं बैठता तो क्या करें?
फत्ते ने निराश होकर कहा।
कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। काठ के बर्तन और खेती के जो उपकरण हमने इधर बनाए हैं, वे कब काम आएंगे? उनके बदले अनाज का जुगाड़ तो कर लें। महीने भर का गुजारा तो किसी-न-किसी तरह हो ही जाएगा। कल सुबह अंधेरे में पास के गांव तक हो आएंगे। चुन्या से भी तैयार रहने को कह देना। वैसे गांव वालों की हालत भी पतली है। फ़िर भी कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा,
गमेर से यह सुनने पर फत्ते अपनी छानी की ओर चला गया और गमेर अपने बनाये बर्तनों और उपकरणों को संभालने में लग गया।
अभी पौ नहीं फटी थी। गमेर, चुन्या और पफत्ते तीनों अंधेरे में ही जंगल से होकर चल पड़े - सिर पर काठ के बर्तन और खेती के उपकरण लादे। पाला इतना पड़ा कि पेड़ों से जैसे पानी बरस रहा था। नंगे बदन वे तीनों राजी बुरी तरह भीग गए। ठण्ड से कांपते-सिकुड़ते और जमीन पर केंचुओं को कुचलते हुए वे आगे बढ़ते रहे। न जाने कितनी जोंकें उनके पैरों की उंगलियों के बीच चिपक गई थीं। खुजली का आभास हो रहा था। पूरब की पहाड़ियों पर लाली क्या फूटी कि वे तीनों एक गांव के निकट थे। पनघट सामने था। वहीं बिछे पत्थरों पर बर्तन आदि रख दिए। फ़िर तीनों एक ऐसी घनी झाड़ी में जाकर छिप गए, जहां से पनघट का सारा दृश्य साफ-साफ दिखाई देता था। चुन्या ने कुछ कहना चाहा तो गमेर ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत कर दिया। आवाज करने से उनकी उपस्थिति का पता जो चल जाता। बेचारे इशारों में ही बतियाते रहे और पैरों से चिपकी जोंकों से पल्ला छुड़ाते रहे।
कुछ और उजास हुआ। गांव की दो औरतें पानी लेने आ पहुंची। राजियों के बर्तनों पर नजर पड़ी। गगरियां भरीं और एक-एक ठेकी भी साथ में लेती गईं। यही क्रम चलता रहा। कुछ ही देर में सारे बर्तन और उपकरण उठ गए थे। मुश्किल से दो-चार लोग ही अनाज लेकर आए। झाड़ी में बैठे राजी निराश होकर वह सब देखते रहे। नजरें बचाकर किसी तरह पत्थरों पर रखा अनाज उठाया, अपनी जाफ़ियों (रेशों से बने थैले) में भरा और छिप-छिपाकर अपने रौत्यूड़ा (रावतों अर्थात् राजियों की जंगली बस्ती) की ओर चल पड़े। रास्ते में फत्ते ने गमेर से कहा-
दाज्यू, यह तो कुछ भी नहीं हुआ।
चुन्या भी बोल उठा-
हम तो लुट गए दाज्यू। दो-तीन महीनों की मेहनत और इतना-सा अनाज!
गमेर ने कहा-
हां,इतने कम की आशा तो मुझे भी नहीं थी। लगता है कुछ लोग बर्तन तो ले गए, पर अनाज लेकर लौटे ही नहीं। इतना तो मैं भी मानकर चला था कि लोगों के हाथ तंग हैं, अनाज कम ही मिलेगा। लेकिन लोग बर्तन उठा ले जाएं और बदले में दो दाने भी न दें, इसकी आशा नहीं थी। ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई, इसी का दु:ख है।
-तो क्या हम इसी तरह लुटते रहेंगे?, चुन्या ने आवेश में आकर पूछा।
कर भी क्या सकते हैं चुन्या? हम हैं ही कितने? वे अगर अपनी पर उतर आएं तो ---? हां, एक ही उपाय है, रजवार अगर चाहें तो बात बन सकती है। उनका आदेश कोई टाल नहीं सकेगा। जब भी मौका मिलेगा अस्कोट जाकर बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं।
गमेर ने समझाया।
चुन्या और फत्ते पहले तो गमेर से सहमत नहीं हुए। मरने-मारने की बात ही बढ़-चढ़कर करते रहे। लेकिन गमेर ने जब उन्हें बताया कि रजवार तो रिश्ते में "भाऊ" (छोटे भाई) लगते हैं, वे कुछ न कुछ जरूर करेंगे। फ़िर हम हैं कितने जो दीगर लोगों का मुकाबला कर सकें? इस पर उनका जोश ठण्डा पड़ गया और वे भी अस्कोट के रजवार के पास जाने की बात मान गए। अदला-बदली के लिए वे दूसरे गांवों में भी गए, लेकिन वही ढाक के तीन पात। बहुत कम अनाज मिल पाया। किसी तरह दिन काटते रहे कि कब जाड़ा शुरू हो और बाहर निकलने का अवसर आए। घर-गृहस्थी के झंझट में वे रजवार से मिलने की बात तो जैसे भूल ही गए। एक दिन फत्ते को याद आई और वे तीनों गमेर की अगुवाई में अस्कोट के लिए चल पड़े।
जाड़े के मौसम की शुरूआत। तीन-चार दिनों से आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। दिगतड़ के उफपर सीराकोट-द्योधुरा, गोरी-रौंतिस के बीच यमस्यारी घणधुरा तथा पूर्वोत्तर में गोरी-पार घानधुरा-पक्षयां पौड़ी और छिपलाकोट की ऊंचाइयों पर सफेद कुहरे की चादर मौसम के और बिगड़ने की सूचना दे रही थी। मौसम की परख आदमी से कहीं अधिक पशु-पक्षियों को होती है। चिफलतरा का गमेर बणरौत अपने दो साथियों - चुन्या और फत्ते के साथ अस्कोट के रजवार से भेंट करने निकला था। तीनों लगभग नंगे थे। केवल अपने गुप्तांग ही किसी तरह ढके हुए। मालू की बेल के रेशे से बने कमरबन्द और उसी के चौड़े पत्तों का उपयोग इस कुशलता से किया गया था कि हरे रंग के मुतके (लंगोट) का आभास होता था।
रौंतिस गाड (नदी) तक आते-आते उन पत्राधारी वनरौतों को अचानक एक काखड़ नीचे की ओर भागता नजर आया। वे समझ गए कि बर्फबारी के डर से जानवर नीचे गरम घाटियों की ओर आ रहे हैं। उनकी बांछें खिल गईं। यदि कोई जानवर हाथ लग गया तो रजवार से खाली हाथ भेंट करने की बेअदबी से तो बच ही जाएंगे। गमेर ने अपने तीर-कमान संभाले और दोनों साथियों को सतर्क नजरों से टोह लेने का इशारा किया। वे एक खेत के किनारे क्वेराल (कचनार) के पेड़ के नीचे खड़े थे। फत्ते ने नीचे की ओर नजर दौड़ाई तो मवा की एक शाखा के नीचे काखड़ को खड़ा पाया और गमेर को इशारा किया। काखड़ की नजर दूसरी ओर थी और गमेर ने जो तीर मारा तो काखड़ नीचे रौंतिस के पानी में जा गिरा। गमेर और फत्ते नीचे भागे ताकि काखड़ को कब्जे में कर सकें। लेकिन चुन्या की नजर तो खेत के किनारे गींठी (बाराही कन्द) खोदते एक साही पर टिकी थी। उसने दोनों हाथों से एक भारी सा पत्थर उठाया और दबे पांव पास जाकर साही पर दे मारा। बेचारे साही को अपने तीरों का उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिला। साही भी हाथ लगा और गींठी भी उसने अपनी जापफी (रेशों से बुनी झोली) के हवाले की। पिफर वह भी गमेर और पफत्ते के पास चला आया। गमेर और फत्ते काखड़ को मालू की बेल से एक लट्ठे पर बांध चुके थे। चुन्या और पफत्ते ने काखड़ अपने कन्धों पर उठाया। गमेर ने चुन्या की जापफी भी अपने कन्धे से लटकाई और वे तीनों रौंतिस-पार अस्कोट के लिए चढ़ाई चढ़ने लगे।
वे छिप-छिपकर चल रहे थे। डर था कि कहीं पड़ोस के बसेड़ा, कन्याल या धामी लोगों में से किसी ने देख लिया तो कहीं काखड़ से हाथ न धोना पड़े। रह-रहकर ठण्डी पछुवा के झोंके चलने लगे थे। उफपर आसमान पर बादल भी गहराने लगे और बरसने-बरसने को हो आए थे। वे अभी उबड़-खाबड़ रौंतिस के किनारे से अधिक दूर नहीं जा पाए थे। अचानक पानी बरसने लगा। तीनों रौंतिस के किनारे एक ओडार (गुफा) की शरण लेने पर बाध्य हो गए। ऊंचाइयों पर सम्भवत: बर्फ पड़ने लगी थी। उधर से आते हवा के ठण्डे झोंके कंप-कंपी पैदा कर रहे थे। सौभाग्य से गुफा में कुछ सूखी लकड़ियां और झाडियां पड़ी मिल गईं। गुफा राजी बण-रौतों की यदा-कदा रात बिताने का आश्रय जो थी। मालू की एक बेल भी अपने चौड़े-चौड़े पत्तों के साथ गुफा के आधे खुले भाग को ढके हुए थी। पानी बरसना नहीं रुका तो अब रात उसी गुफा में काटनी थी। चुन्या ने मालू के पत्तों के बीच से बाहर झांका और बोला -
थिप्पे पौवा,(शाम हो गई है)।
ओअं, दे अस्कोट हं पियरे हूँर (हां, आज तो अस्कोट नहीं पहुंच पाएंगे), गमेर ने कहा।
उन्होंने काखड़ का शव गुफा की पिछली दीवार के सहारे एक पत्थर पर रख दिया था। गमेर ने अपनी जापफी से अगेला (आग पैदा करने वाला लोहे का टुकड़ा), डांसी (चकमक और कसबुलु ;एक वन्य पौधा जिसके पत्तों की सफेद परत को रेशों के रूप में उतार लिया जाता है, पुराना होने पर वह रेशा शीघ्रता से आग पकड़ लेता है) निकाले। डांसी से चिनगारियां निकली और कसबुलु ने आग पकड़ ली। सूखी पत्तियों, झाड़ियों और लकड़ियों के बीच रखकर हवा दी तो आग भड़क उठी और तीनों बैठकर आग सेंकने लगे। ठण्ड इतनी अधिक थी कि एक ओर जहां ताप का अनुभव होता, वहीं शरीर का दूसरा भाग सुन्न पड़ता महसूस होता। वे बारी-बारी से आग की ओर कभी मुंह करते तो कभी पीठ और इस तरह ठण्ड से बचने का प्रयास करते रहे। अंधेरा और गहराने पर गमेर ने दांत किट-किटाते चुन्या और फत्ते से कहा -
दे हं चुजावरे हूँर?(आज खाने का क्या होगा?)
चुन्या ने जवाब में अपनी जापफी से साही निकाला। उसके तीर जैसे कांटे उखाड़े और पत्थर के आघात से दो-तीन टुकड़े कर दिए। फत्ते तब तक मालू के साबुत पत्ते चुन चुका था। साही के टुकड़े मालू के पत्तों में लपेटकर धधकती आग में भूनने रख दिए गए और गीठी भी गरम राख में दबा दी गई। कुछ देर में मांस और गींठी दोनों पक गए। कुछ ठण्डे होने पर बिना नमक के ही वे तीनों मांस और गींठी का स्वाद लेने लगे। खाना समाप्त होते ही तीखी ठण्डी हवा फ़िर से सताने लगी। फत्ते ने आग को और धधकाने का प्रयास किया। किन्तु अब लकड़ियां समाप्त होने को थीं, केवल शोले भर रहे गए थे और उनसे तपन उस मात्रा में नहीं मिल पा रही थी, जितनी पहले लपटों से मिल रही थी। तीनों सटकर इस तरह बैठ गए कि एक-दूसरे के शरीर की गर्मी से ठण्ड का प्रकोप शान्त कर सकें। गमेर ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए गम्भीर होकर कहा-
बाप रे! यह हाल तो हमारा है, बेचारे गरीब-गुरबों का क्या होगा?